कंप्यूटर एक परिचय
THE WEBZONE CYBER
आधुनिक युग के विकास में कंप्यूटर का योगदान अतुल्यनीय रहा है, फिर चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आज कंप्यूटर की मौजूदगी हर कहीं सहजता से देखी जा सकती है| आज हमारे रोजमर्रा के हर कार्य कंप्यूटर पर ही निर्भर करते हैं, रेल तिकट आरक्षित करना हो या ATM मशीन से कुछ रुपये निकालनें हों, या चाहे फोटो ही क्यों ना खिंचवानी हो ये सभी कार्य आज कंप्यूटर के जरिये बड़ी ही आसानी से एवं कम समय में और तो और कम लागत में हो जाता है|
विज्ञान, तकनीकी, शोध, चिकित्सा, प्राद्योगिकी, उड्डयन, संचार एवं शिक्षा के साथ-साथ कंप्यूटर ने कृषि के क्षेत्र की प्रगति में भी बड़ी अहम् भूमिका अदा की है| आज कंप्यूटर क्रांति ने मानों सारे विश्व को एक सूत्र में बाँध दिया है| इन्टरनेट ने तो कंप्यूटर के प्रचार-प्रसार में बड़ा ही अहम् भूमिका निभाया है| आज हम इन्टरनेट के जरिये दुनिया के एक कोने से दुसरे कोने में पलक झपकने भर में ही संपर्क साध सकते हैं, ई-मेल ने तो पत्र-व्यवहार का काया-कल्प ही कर दिया है| जहाँ साधारण डाक द्वारा पत्राचार की प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे, वहीँ आज ई-मेल के जरिये संदेश चंद सेकंड्स में ही दुनिया के किसी भी कोने में बड़ी ही आसानी से भेजे जा रहे हैं; और तो और आप इन्टरनेट टेलेफोनी के जरिये कहीं से-कहीं भी बातें कर सकते हैं एकदम वैसे ही जैसे हम टेलेफोन के जरिये करते हैं|
जिस तेजी से एवं इतने कम समय में कंप्यूटर का विकास हुआ है, इतनी तेजी से दुनिया का दूसरा कोई भी विकास नही देखा गया, इसे हम क्रांति नहीं तो और क्या कहेंगे! यही वजह है की यह युग "कंप्यूटर का यूग" के नाम से जाना जाता है! आम भाषा में कहें तो आज हर एक वस्तु का कंप्यूटरीकरण हो गया है| कंप्यूटर ने हर क्षेत्र को एक नया आयाम दे दिया है| शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने क्रांति कर दिया है| आज पाठ्यक्रम में कंप्यूटर एक अहम् एवं अनिवार्य हिस्सा बन गया है| यहाँ तक कि कंप्यूटर ने बच्चों के खेल में भी अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है, विडियो/कंप्यूटर गेम्स बच्चों में ही नहीं अपितु बड़ों में भी बेहद ही लोकप्रिय हो चला है| संगीत सुनना हो या फिर कोई फ़िल्म देखनी हो या फिर चित्रकारी ही क्यों ना करनी हो कंप्यूटर के द्वारा ये सब सम्भव है| यही खूबी कंप्यूटर को "हर कार्य सक्षम" का प्रमाण प्रदान कराती है|
जिस प्रकार हम बिजली एवं अन्य संसाधनों के बिना जीवन कि कल्पना नहीं कर सकते उसी प्रकार आज के युगमें हम कंप्यूटर के बिना रोजमर्रा होने वाले कार्यों कि कल्पना भी नही कर सकते|
कंप्यूटर की संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली अंग्रेजी में होने की वजह से आम हिन्दी भाषियों को कंप्यूटर समझने एवं उस पर कार्य कराने में काफ़ी दिक्कत होती रही है, कंप्यूटर समझने और उस पर कार्य करने के लिए अंग्रेजी भाषा का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से कंप्यूटर की पहुँच हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषियों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत हद तक सम्भव भी हुआ है| आज कंप्यूटर सिर्फ़ अंग्रेज़ी भाषा तक सिमित नहीं रहा, बल्कि अब वह भारतीय ही नहीं अपितु दुनिया की अन्य कई महत्वपूर्ण भाषाओँ में भी फल-फुल रही है और अपनी पहुँच हर किसी तक पहुँचाने में सक्षम हुई है|
कंप्यूटर - कार्यप्रणाली
कंप्युटर कल पुर्जो से बना हुआ एक मशीन मात्र है| कंप्यूटर के पास अपना स्वयं का कोई दिमाग या चेतना नहीं होता है| तो आख़िर वह इतने सारे कार्य कैसे कर लेता है?
कंप्यूटर को कार्यशील बनाने के लिए उसके कलपुर्जो के अलावा उसमें एक विशेष प्रकार के संदेश अर्थार्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है| सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर अपने से जूडे हर एक उपकरण से उनके लिए निर्धारित किए गए कार्य करवाता है| किसी उपकरण को कैसे कार्य में लाना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अन्दर पहले से ही स्थापित की हुई होती है| कंप्यूटर के प्रोसेसर में अपार शक्ति एवं क्षमता होती है परन्तु सॉफ्टवेयर के निर्देश के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता, उसे चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो प्रोसेसर , मदरबोर्ड, रैम हार्डडिस्क, फ्लॉपी ड्राइव , सीडी रोम एवं अन्य सभी डिवाइसेस के बिच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को आत्मसार करता करता है अर्थात कंप्यूटर को जीवन प्रदान करता है| इस विशेष सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है|
"कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए कार्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्देशानुसार विश्लेषण कर अपेच्छित जानकारी उपलब्ध कराता है|"
यह पुरी प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है|
१) इनपुट (Input) - कुंजीपटल (KeyBoard) द्वारा कंप्यूटर में तथ्य भरना तथा अपेच्छित कार्य बताना|
२) प्रोसेसिंग (Proccessing) - CPU द्वारा उपलब्ध तथ्यों का निर्देशानुसार विश्लेषण करना|
३) आउटपुट (Output) - विश्लेषण द्वारा उपलब्ध जानकारी को दृश्यपटल (Screen) पर दर्शाना या मुद्रक यंत्र (Pinter) द्वारा मुद्रण (Print) करना|
4) संरक्षण (Storage) - विश्लेषण द्वारा उपलब्ध जानकारी को संरक्षण उपकरण (Storage Device) पर संरक्षित करना|
कंप्यूटर को कार्यशील बनाने के लिए उसके कलपुर्जो के अलावा उसमें एक विशेष प्रकार के संदेश अर्थार्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है| सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर अपने से जूडे हर एक उपकरण से उनके लिए निर्धारित किए गए कार्य करवाता है| किसी उपकरण को कैसे कार्य में लाना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अन्दर पहले से ही स्थापित की हुई होती है| कंप्यूटर के प्रोसेसर में अपार शक्ति एवं क्षमता होती है परन्तु सॉफ्टवेयर के निर्देश के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता, उसे चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो प्रोसेसर , मदरबोर्ड, रैम हार्डडिस्क, फ्लॉपी ड्राइव , सीडी रोम एवं अन्य सभी डिवाइसेस के बिच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को आत्मसार करता करता है अर्थात कंप्यूटर को जीवन प्रदान करता है| इस विशेष सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है|
"कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए कार्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्देशानुसार विश्लेषण कर अपेच्छित जानकारी उपलब्ध कराता है|"
यह पुरी प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है|
१) इनपुट (Input) - कुंजीपटल (KeyBoard) द्वारा कंप्यूटर में तथ्य भरना तथा अपेच्छित कार्य बताना|
२) प्रोसेसिंग (Proccessing) - CPU द्वारा उपलब्ध तथ्यों का निर्देशानुसार विश्लेषण करना|
३) आउटपुट (Output) - विश्लेषण द्वारा उपलब्ध जानकारी को दृश्यपटल (Screen) पर दर्शाना या मुद्रक यंत्र (Pinter) द्वारा मुद्रण (Print) करना|
4) संरक्षण (Storage) - विश्लेषण द्वारा उपलब्ध जानकारी को संरक्षण उपकरण (Storage Device) पर संरक्षित करना|

कंप्यूटर की विशेषताएं
आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता महत्त्वपूर्ण साबित हो रही है| हर कहीं कंप्यूटर का बोल-बाला ऐसे ही नहीं है, कंप्यूटर की अपार सपफलता का राज़ उसकी कई विशिष्ट खूबियाँ हैं|कंप्यूटर की कुछ प्रमुख विशेषताएं:
१) स्वचलित (Automation): कंप्यूटर की संरचना इस प्रकार की गयी है की वो दिए गए कार्य को किसी भी प्रकार के बाहरी सहायता के स्वयं ही उसमें दर्ज निर्देशानुसार पुरा करता है और हमें इच्छित परिणाम देता है| परन्तु ऐसा बिल्कुल नहीं है की कंप्यूटर हमारी ही तरह समझबूझ रखता है अथवा स्वावलंबी होता है, कंप्यूटर में किसी भी कार्य को सुचारू रूप से दिए गए निर्देशों के आधार पर कैसे पुरा करना है इसकी जानकारी पहले से ही भरी हुई होती है, जिसकी सहायता से वह कार्य करता है| कंप्यूटर में तरह-तरह के कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के प्रोग्राम/सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कोई कार्य कैसे करना है उसकी जानकारी पहले से ही भरी हुई होती है|
भिन्न-भिन्न कार्यों को करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं|
२) तीव्रता (Speed): कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की गणना को पलकभर में ही हल करने की क्षमता होती है, जटिल से जटिल प्रकार की गणनाएं वह बड़ी ही तीव्रता एवं पुरी सटीकता से पुरा करता है| कई प्रकार की गणितीय/भौमितिक/भौगोलिय/वैज्ञानिक/आकाशीय आदि गणनाएँ जिन्हें पुरा करने में हमें कई वर्षों यहाँ तक की पुरा जीवन भी लग सकता हैं, उन्हें कंप्यूटर कुछ ही क्षणों में बड़ी ही सरलता से पुरा कर लेता है|
हम किसी यात्रा की दुरी को तय करने की तीव्रता, प्रति घंटा कितनी दुरी तय की गयी इस प्रकार आंकते करते है, किसी कार्य को पुरा करने में जितना समय लगता है वह उस कार्य को करने की तीव्रता दर्शाता है| कंप्यूटर के कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकंड्स, प्रति मिलिसेकंड्स, प्रतिमाइक्रो सेकंड्स, प्रति नेनोसेकंड्स ईत्यादी में आंकी जाती है, कंप्यूटर लाखों-करोणों निर्देश प्रतिसेकंड्स की दर से करने में सक्षम है|
कंप्यूटर के तीव्रता को मापने की इकाई निम्नलिखित हैं:
i) kIPS: Kilo Instructions Per Second
i) MIPS: Million Instructions per second
ii) megaflop, MFLOP: Million Floating Point Operations per second
iii) teraflop: Trillion Floating Point Operations per second

[इकाई =
1 kilo = १००० या १०३,
1 Million = १० लाख या १०६;
1 Billion = १ अरब या १०९,
1 Trillion= १० खरब या १०१२]
३)सटीकता (Accuracy): कंप्यूटर हर कार्य तीव्रता से तो करता ही है, साथ ही साथ हर परिणाम की सटीकता भी बरकरार रखता है। चूँकि कंप्यूटर एक यंत्र है, इसलिए वो जो भी कार्य करता है उसे निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर ही करता है, जिससे की किसी भी प्रकार के चूक की संभावना न के बराबर होती है| यदि कंप्यूटर किसी कार्य का गलत परिणाम देता है तो भी उसमें कंप्यूटर की जरा भी गलती नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाये गए प्रोग्राम द्वारा निर्दिष्ट निर्देश का पालन करके ही किसी कार्य को अंजाम देता है, तो यदि कोई त्रुटी होती भी है तो उसे इंसानी भूल ही कहा जायेगा| सम्भवत: प्रोग्राम लिखते समय प्रोग्रामर से ही कोई त्रुटी हो जाती है, जिसके फलत: कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम गलत हो|
४) संचयन (Memory & Storage): कंप्यूटर में हर तरह के जानकारी एवं आंकडों को संचित व स्मरण रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है| जब भी किसी जानकारी की जरुरत होती है कंप्यूटर उसे तुंरत ही संचित जानकारी में से हासिल कर लेता है| रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रतिदिन हजारों जानकारी एवं अनुभवों से गुजरते है, परन्तु हमारा मस्तिष्क उन सभी जानकारी व अनुभवों को सदा के लिए संचित नहीं रखता, जो भी अनुभव या जानकारी हम याद रखना चाहते हैं हमारा मस्तिष्क उन्हें ही संचित करता है तथा गैरजरूरी जानकारी को सन: सन: हमारी याददास्त से निकालता जाता है| परन्तु कंप्यूटर में आंकडों को लंबे समय तक याद/संचित रखनें के लिए एक विशिष्ट युक्ति होती है जिसे द्वितीय मेमरी (Secondory Storage Device) कहते हैं| एक बार जो भी जानकारी संरक्षित कर दिया जाता है वह फिर सदा के लिए बना रहता है, वह तभी मिटता है जब की उपयोगकर्ता स्वयं ही उसे नहीं मिटा देता|
५) क्षमता एवं उत्पादकता (Diligence): कंप्यूटर हर कार्य बड़ी ही संजीदगी से करते हैं, उन्हें हमारी तरह कभी भी थकान महसूस नहीं होती| एक ही प्रकार के कार्य करते करते इंसान उब सकते जिससे उनकी उत्पादकता तथा गुणवत्ता का स्तर घट सकता है, उसके विपरीत कंप्यूटर में एक ही काम बिना रुके लगातार करने की क्षमता होती है, और वे उत्पादकता एवं गुद्वात्ता से जरा भी समझौता नहीं करते| वे एक ही बार में कई तरह के कार्य कर सकते हैं, उनमें अपार शक्ति होती है| जो कार्य कई लोगों को मिलकर पुरा करने में महीनों लग सकते हैं उन्हें कंप्यूटर चुटकी बजाते ही पुरा कर सकने में सामर्थ्यवान होते हैं|
६) बहुमुखी प्रतिभा (Versatility): कंप्यूटर विविध प्रकार के कार्य करने में पारंगत होते हैं| चाहे जटील से जटील गणितीय गणनाएँ करना हो, किसी जानकारी का अवलोकन करना हो, मौसम का हाल जानना हो, दूरध्वनी का प्रषारण करना हो, चिकित्सकीय इलाज करना हो, दस्तावेज तैयार करना हो ऐसे कई कार्य कंप्यूटर बड़ी ही आसानी से पुरा कर लेता है| मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर कही ही एक रूप है, इनका उपयोग सिर्फ किसी से संपर्क साधने तक ही सिमित नहीं रहा, अब ये भी एक साथ कई कार्य कर सकने में सक्षम होते हैं|
निर्देशों की सूचि जिसे प्रोग्राम कहते हैं, का क्रियान्वयन और प्राप्त जानकारी को रक्षित करनें करनें की क्षमता ही कंप्यूटर को सबसे अलग बनती है, कंप्यूटर की यही विशेषता इसे एक कैलकुलेटर से भिन्न बनती है |
७) भवनाहीनता (No Feelings): हम इंसानों की तरह कंप्यूटर की अपनी कोई भावना या चेतना नहीं होती| किसी कार्य को निरंतर करते रहने पर भी उसे चिढ़, थकान या उबन नहीं होती| चूँकि कंप्यूटर कलपुर्जों से बना एक मशीन मात्र है इसलिए उसे कभी भी खुशी, दुःख या उत्तेजना महसूस नहीं होती|
८) बुद्धिहीनता (Absence of IQ): कंप्यूटर की अपनी कोई बुध्धिमत्ता नहीं होती| कंप्यूटर किसी भी प्रकार की व्यवहारिक या आतंरिक गड़बडी को कैसे दुर करना है इसका निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, इसके लिए उसे उपयोगकर्ता के निर्देश पर निर्भर रहना पड़ता है| कंप्यूटर स्वयं चालू-बंद नहीं हो सकता| कंप्यूटर छोटे बच्चों की तरह ही होत हैं, वे बिलकुल वैसा ही करते हैं जैसा की हम चाहते हैं या\और उन्हें सिखाते या बताते हैं|
कंप्यूटर - उत्पत्ति एवं क्रमागत उन्नति
आप अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कितने आविष्कार के बारे में सोच सकते हैं, जो हमारे समाज में सब कुछ बदल कर रख दे? कंप्यूटर ने चंद दशकों में ही पुरी दुनिया के सोचने-समझने, कार्य करने और यहाँ तक की रहन-सहन का तरीका भी बदल के रख दिया| इसे कंप्यूटर क्रांति माना जाने लगा| परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता की कंप्यूटर की खोज इसी सदी में हुई, अंकों एवं गणन का उपयोग मानवजाति के विकास क्रम के शुरुवात से ही रहा है| शुरुवाती दौर में, हाथों की उँगलियों का उपयोग करना, मृत प्राणियों के हड्डी का प्रयोग करना, रेखाएं खींचना, चिन्ह बनाना इत्यादि का उपयोगहोता था|


अब तक ज्ञात श्रोतों के आधार पर, शुन्य के इस्तेमाल का सर्वप्रथम उल्लेख हिंदुस्तान के प्राचीन खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभठ्ठ द्वारा रचित गणितीय खगोलशास्त्र ग्रंथ आर्यभठ्ठीय के संख्या प्रणाली में, शून्य तथा उसे दर्शाने का विशिष्ट संकेत सम्मिलित किया था, तभीसे से संख्याओं को शब्दों में प्रदर्शित करने के चलन शुरू हुआ|

भारतीय लेखक पिंगला (200 ई.पू.) नें छंद शास्त्र का वर्णन करने के लिए, उन्नत गणितीय प्रणाली विकसित किया और द्विआधारिय अंक प्रणाली (०,१)(Binary Number System) का सर्वप्रथम ज्ञात विवरण प्रस्तुत किया| इसी जादुई अंक अर्थात अंक ० तथा अंक १ का प्रयोग कम्प्यूटर की संरचना में प्रमुख रूप से किया गया|
"कंप्यूटर" शब्द का चलन आधुनिक कंप्यूटर के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से ही होता रहा है, पहले जटील गणनाओं को हल करने के लिए उपयोग होने वाले अभियांत्रिकी मशीनों को चलाने वाले विशेषज्ञ को "कंप्यूटर" कहा जाता था| ऐसे जटील अंकगणितीय सवाल, जिन्हें हल करना बेहद मुश्किल ही नहीं अपितु अत्यधिक समय लेने वाला भी होता था, को हल करनें के लिए मशीनों का आविष्कार हुआ, और समय के साथ-साथ उनमें कई बदलाव व सुधार होते गए| विज्ञान की खोज और उसमें हुए कई महत्त्वपूर्ण आविष्कारों ने कंप्यूटर के आधुनिककरण में खूब योगदान दिया है| गणन यन्त्र विशेषज्ञों से आगे बढ़कर अभियांत्रिक मशीनों का बनना, विद्युतचालित यंत्रों का आविष्कार और फिर आधुनिक कंप्यूटर का स्वरूप मिलना, ये कंप्यूटर आविष्कार के क्रमागत उन्नति पथ हैं|
३००० ई.पु. में "ABACUS" नामक गणना करने वाले यन्त्र का उल्लेख किया जाता है, ABACUS में कई छडें होती हैं जिनमें कुछ गोले होते हैं जिनके जरिये जोड़ व घटाना करते थे, परन्तु इनसे गुणन या विभाजन नहीं किया जा सकता था|

 १६००वीं सदी से लेकर 1970 तक का दशक कंप्यूटर के विकास में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा है|
१६००वीं सदी से लेकर 1970 तक का दशक कंप्यूटर के विकास में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा है|*१६२२वीं ईसवी में विलियम औघ्त्रेड ने "स्लाइड रुल" का ईजाद किया|
*१६४२वीं ईसवी में ब्लैसे पास्कल नें पास्कलिन नमक यन्त्र बनाया जिससे जोड़-घटना किया जा सकता था|
*१६७२वीं ईसवी में Gottfried Wilhelm Leibniz नें Leibniz Step Reckoner (or Stepped Reckoner) नामक एक कैलकुलेटर मशीन बनाया जिसमे जोड़, घटाना, गुना तथा भाग ये सभी गणनाएं करना सम्भव हुआ|

*१८२२ ईसवी में चार्ल्स बैबेज नें "डिफरेंशिअल इंजन" का आविष्कार किया तथा १८३७ ईसवी में "एनालिटिकल इंजीन " का अविष्कार किया जो की धनाभाव के कारण पुरा न हो सका, कहा जाता है की तभी से आधुनिक कंप्यूटर की शुरुवात हुई| ईसलिए चार्ल्स बैबेज को "कंप्यूटर का जनक " भी कहा जाता है|


* १९४१ ईसवी में "कोनार्ड जुसे" नें zuse-Z3 का निर्माण किया, जो की द्विआधारी अंकगणितीय (Binary Arithmetic) एवं चल बिन्दु अंकगणितीय (Floating point Arithmetic) संरचना पर आधारित सर्वप्रथम विद्युतीयकंप्यूटर था|
 * १९४६ में अमेरिकी सैन्य शोधशाला ने "ENIAC" (Electronic Numerical Integrator And Computer) का निर्माण किया जो की दशमिक अंकगणितीय (Decimal Arithmetic) संरचना पर आधारित सर्वप्रथम कंप्यूटर बना| जो आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर के विकास का आधार बना|
* १९४६ में अमेरिकी सैन्य शोधशाला ने "ENIAC" (Electronic Numerical Integrator And Computer) का निर्माण किया जो की दशमिक अंकगणितीय (Decimal Arithmetic) संरचना पर आधारित सर्वप्रथम कंप्यूटर बना| जो आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर के विकास का आधार बना| * १९४८ में Manchester Small-Scale Experimental Machine पहला ऐसा कंप्यूटर बना जो की किसी प्रोग्राम को Vaccum Tube में संरक्षित कर सकता था|
* १९४८ में Manchester Small-Scale Experimental Machine पहला ऐसा कंप्यूटर बना जो की किसी प्रोग्राम को Vaccum Tube में संरक्षित कर सकता था| आगे चलकर इस प्रगति पथ में और भी कई विशेष परिवर्तन हुए और आधुनिक कंप्यूटर चलन में आया|
आगे चलकर इस प्रगति पथ में और भी कई विशेष परिवर्तन हुए और आधुनिक कंप्यूटर चलन में आया|कंप्यूटर पीढियाँ
ZUSE-Z3 एवं ENIAC को कम्प्युटर के विकास का आधार मानें तो तब से लेकर अब तक कम्प्युटर विकासक्रम में कई पड़ाव आए, सर्वाधिक महत्त्वपूर्णता के आधार पर अबतक कंप्यूटर की कुल पाँच पीढियाँ हुई हैं|
विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अविष्कार कम्प्युटर के प्रगति पथ में बहुत सहयोगी रहे हैं| हर पीढ़ी में कम्प्युटर की तकनीकी एवं कार्यप्रणाली में कई आश्चर्यजनक एवं महत्त्वपूर्ण आविष्कार हुए, जिन्होंने कम्प्युटर तकनीकी की काया पलट कर दी| हर पीढ़ी के बाद कम्प्युटर की आकार-प्रकार, कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षमता में सुधार होते गए| कम्प्युटर का विकास दो महत्वपूर्ण भागों में साथ-साथ विकास हुआ, एक तो आतंरिक संरचना एवं हार्डवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेर, दोनों एक दुसरे पर निर्भर होने के साथ ही साथ एक दुसरे के पूरक भी हैं| जैसे-जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कम्प्यूटर क्षेत्र में तरक्की हुई उनकी मांग भी बढ़ने लगी और वे पहले की अपेक्षा सस्ते भी होते गए, आज कम्प्युटर घर-घर में पहुंचनें की वजह उनका किफायती होना ही है|
कम्प्युटर के पीढियों की कुछ आधारभूत जानकारी इस प्रकार है,
१) पहली पीढ़ी (१९४१ से १९५४) [आधार - वैक्युम ट्यूब]:
विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अविष्कार कम्प्युटर के प्रगति पथ में बहुत सहयोगी रहे हैं| हर पीढ़ी में कम्प्युटर की तकनीकी एवं कार्यप्रणाली में कई आश्चर्यजनक एवं महत्त्वपूर्ण आविष्कार हुए, जिन्होंने कम्प्युटर तकनीकी की काया पलट कर दी| हर पीढ़ी के बाद कम्प्युटर की आकार-प्रकार, कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षमता में सुधार होते गए| कम्प्युटर का विकास दो महत्वपूर्ण भागों में साथ-साथ विकास हुआ, एक तो आतंरिक संरचना एवं हार्डवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेर, दोनों एक दुसरे पर निर्भर होने के साथ ही साथ एक दुसरे के पूरक भी हैं| जैसे-जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कम्प्यूटर क्षेत्र में तरक्की हुई उनकी मांग भी बढ़ने लगी और वे पहले की अपेक्षा सस्ते भी होते गए, आज कम्प्युटर घर-घर में पहुंचनें की वजह उनका किफायती होना ही है|
कम्प्युटर के पीढियों की कुछ आधारभूत जानकारी इस प्रकार है,
१) पहली पीढ़ी (१९४१ से १९५४) [आधार - वैक्युम ट्यूब]:
- अपने समय के ये सर्वाधिक तेज कम्प्यूटर थे| कम्प्युटर की संरचना में कई हजार वक्क्यूम ट्यूब का मुख्य रूपसे इस्तेमाल किया गया|
- जिस वजह से इनके द्वारा बिजली की खपत बहुत अधिक होती थी|
- कई हजार वक्क्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होने के कारण अत्याद्धिक उर्जा उत्पन्न होती थी|

- वैक्यूम ट्यूब में उपयोग में लिए जाने वाले नाज़ुक शीशे के तार अधिक उर्जा से शीघ्र ही जल जाते थे| इनकेबाकि कलपुर्जे जल्दी ही ख़राब हो जाते जिससे उन्हें तुंरत बदलना पड़ता था, इनके रख रखाव पर विशेष धयान देना पड़ता था|
- जिस वजह से इन्हे जहाँ कहीं स्थापित किया जाता था वहाँ सुचारू रूप से वताकुलन की व्यवस्था करनी पड़ती थी|
- RAM के मैमरी लिए विद्युतचुम्बकीय प्रसार (Relay) का उपयोग किया गया|
- ये मशीनी भाषा पर निर्भर होते थे, जो निम्नतम स्तर के प्रोग्रामिंग भाषा के निर्देशों के आधार पर कार्य करते थे|
- इनके उपयोग के लिए उपयुक्त निर्देश (PROGRAM) लिखना बेहद ही जटील होता था जिस वजह से इनकाव्यावसायिक उपयोग कम होता था|
- इनपुट के लिए इनमें पंचकार्ड एवं पेपरटेप का उपयोग किया जाता था, और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कियाजाता था|
- इनका आकार बहुत बड़ा होता था, जिस कारण इन्हें बड़े-बड़े कमरों में रखा जाता था, जिस वजह से इनका उत्पादन लागत बहुत ही अधिक था|
- ZUSE-Z3, ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAK, IBM 701 आदि मशीन प्रमुख रहे|

- सन् १९४७ में Bell Laboratories नें 'ट्रांजिस्टर' नामक एक नई switching device का आविष्कार किया जोइस पीढी के लिए वरदान से कम नहीं था|
-
ट्रांजिस्टर Germanium Semiconductor पदार्थ से बनते थे जिससे इनका आकार
काफी छोटा होता था, परिणाम स्वरूप वैक्युम ट्यूब की जगह Switching device
का उपयोग होने लगा|

- ट्रांजिस्टर की स्विचिंग प्रणाली बेहद तीव्र थी, जिससे उनकी कार्यक्षमता वैक्युम ट्यूब के मुकाबले बेहद तीव्रहोती थी|
- हालांकि प्रथम पीढी के मुकाबले इनसे कम उर्जा निकलती थी फिर भी ठंडक बनाये रखने के लिए वातानुकूलनकी व्यवस्था अब भी जरुरी था|
- इनकी मैमरी में विद्युतचुम्बकीय प्रसार की जगह चुम्बकीय अभ्यंतर का उपयोग हुआ, जिससे निर्देशों कोमैमरी में ही स्थापित करना हुआ| प्रथम पीढी के मुकाबले इनकी संचयन क्षमता कहीं ज्यादा थी|
- गूढ़ मशीनी भाषा की जगह इनमें उपयोग के लिए सांकेतिक\असेम्बली भाषा का उपयोग हुआ, जिससे निर्देशोंको शब्दों में दर्ज करना सम्भव हुआ|
- COBOL, ALGOL, SNOBOL, FORTRAN जैसे उच्चस्तरीय प्रोगामिंग भाषा तथा क्रमागत प्रचालन तंत्र (Batch Operating System) इसी दौरान अस्तित्व में आए|
- इनका उत्पादन लागत कम हुआ, फलस्वरूप इनका व्यावासिक उपयोग औसत दर्जे का होने लगा|
- यह चरण कम्प्युटर के विकास में बेहद ही रोमांचकारी रहा, अब तक के विकास पथ पर इतनि क्रांति पहले कभी नहीं आयी थी| इंटिग्रेटेड सर्किट IC, जो की कई सारे ट्रांसिस्टर्स, रेसिस्टर्स तथा कैपसीटर्स इन सबको एक ही सिलिकोन चिप पर इकठ्ठे स्थापित कर बनाये गए थे, जिससे की तारों का इस्तेमाल बिलकुल ही ख़त्म हो गया|
 परिणामस्वरूप अधिक उर्जा का उत्पन्न होना बहुत ही घट गया, परन्तु वताकुलन की व्यवस्था अब भी जरुरी बना रहा|
परिणामस्वरूप अधिक उर्जा का उत्पन्न होना बहुत ही घट गया, परन्तु वताकुलन की व्यवस्था अब भी जरुरी बना रहा|- लगभग १० इंटिग्रेटेड सर्किटों को सिलिकोन की लगभग ५ मिमी सतह पर इकठ्ठे ही स्थापित करना संभव हुआ, इसलिए IC को "माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स" तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है|
- इसे "स्माल स्केल इंटीग्रेशन" (SSI) जाना जाता है| आगे जाकर लगभग १०० इंटिग्रेटेड सर्किटों को सिलिकोन चिप की एक ही सतह पर इकठ्ठेही स्थापित करपाना संभव हुआ, इसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन (MSI) जाना जाता है|
- तकनीकी सुधारे के चलते इनकी मैमरी की क्षमता पहेले से काफी बढ़ गयी, अब लगभग ४ मेगाबाईट तक पहुँचगयी| वहीँ मग्नेटिक डिस्क की क्षमता भी बढ़कर १०० मेगाबाईट प्रति डिस्क तक हो गयी|
- इनपुट के लिए कुंजीपटल का एवं आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग होने लगा|
- उच्चस्तरीय प्रोगामिंग भाषा में सुधार एवं उनका मानकीकरण होने से एक कम्प्युटर के लिए लिखे गए प्रोग्राम को दुसरे कम्प्युटर पर स्थापित कर चलाना सम्भव हुआ| FORTRAN IV, COBOL, 68 PL/1 जैसे उच्चस्तरीय प्रोगामिंग भाषा प्रचलन में आये|
- इनका आकर प्रथम एवं द्वितीय पीढी के कम्प्युटर की अपेक्षा काफी छोटा हो गया|
- जिससे मेनफ्रेम कम्प्युटर का व्यावासिक उत्पादन बेहद आसान हो गया और इनका प्रचलन भी बढ़ने लगा| इनके लागत में भी काफी कमी हुयी| जिसके परिणाम स्वरूप ये पहले के मुकाबले बेहद सस्ते हुए|
- माइक्रोप्रोसेसर
के निर्माण से कम्प्युटर युग का कायापलट इसी दौर में शुरू हुआ, MSI
सर्किट का रूपांतर LSI एवं VLSI सर्किट में हुआ जिसमे लगभग ५००००
ट्रांसिस्टर एक चिप पर इकठ्ठे स्थापित हुए|
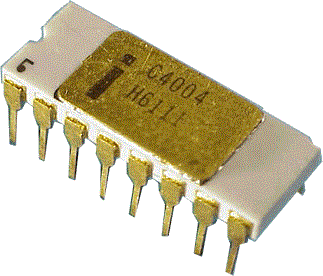
- तृतीय पीढ़ी के कम्प्युटर के मुकाबले इनकी विद्युत खपत बेहद घट गयी| एवं इनसे उत्पन्न होने वाली उर्जा भी कम हुयी| इस दौर में वताकुलन का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं रहा|
- इनके मैमरी में चुम्बकीय अभ्यंतर की जगह सेमीकंडक्टर मैमरी कण प्रयोग होने लगा, जिससे इनकी क्षमता में बहुत वृद्धि हुयी| हार्ड डिस्क की क्षमता लगभग १ GB से लेकर १०० GB तक बढ़ गयी|
- माइक्रोप्रोसेसर तथा मैमरी के अपार क्षमता के चलते, इस दौर के कम्प्युटर की कार्य क्षमता बेहद ही तीव्र हो गयी|
- इस दौर में C भाषा चलन में आयी जो आगे चलकर C ++ हुयी, इनका उपयोग मुख्यरूप से होने लगा| प्रचालन तंत्र (Operating System) में भी काफी सुधार हुए, UNIX, MS DOS, apple's OS, Windows तथा Linux इसी दौर से में चलन में आये|
- कम्प्युटर नेटवर्क ने कम्प्युटर के सभी संसाधनों को एक दुसरे से साझा करने की सुविधा प्रदान की जिससे एक कम्प्युटर से दुसरे कम्प्युटर के बिच जानकारियों का आदान-प्रदान संभव हुआ|
- पर्सनल कम्प्युटर तथा पोर्टेबल कम्प्युटर इसी दौर से चलन में आया, जो की आकार में पिछली पीढी के कम्प्युटर से कहीं अधिक छोटा, परन्तु कार्यशक्ति में उनसे कहीं ज्यादा आगे था|
- इनका उत्पादन लागत बेहद ही कम हो गया जिससे इनकी पहुँच आम लोगों तक संभव हुयी|
५) पांचवीं पीढ़ी (१९९० से अब तक [आधार: ULSI]):
- माइक्रोप्रोसेसर
की संरचना में VLSI की जगह UVLSI चिप का प्रयोग होने लगा| माइक्रोप्रोसेसर
की क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से ईजाफा हुआ, यहाँ तक की ४ से ८ माइक्रोप्रोसेसर एक साथ एक ही चिप में स्थापित होने लगे, जीससे ये अपार शक्तिशाली हो गए हैं|

 इनकी
मेमरी की क्षमता में भी खूब ईजाफा हुआ, जो अब तक बढ़कर ४ GB से भी ज्यादा
तक हो गयी है| हार्ड डिस्क की क्षमता २ टेरा बाईट से भी कहीं ज्यादा तक
पहुच गयी है|
इनकी
मेमरी की क्षमता में भी खूब ईजाफा हुआ, जो अब तक बढ़कर ४ GB से भी ज्यादा
तक हो गयी है| हार्ड डिस्क की क्षमता २ टेरा बाईट से भी कहीं ज्यादा तक
पहुच गयी है|- इस दौर में मेनफ्रेम कम्प्युटर पहले के दौर के मेनफ्रेम कम्प्युटर से कई गुना ज्यादा तेज एवं क्षमतावान हो गए|
- पोर्टेबल कम्प्युटर का आकर पहलेसे भी छोटा हो गया जिससे उन्हें आसानी से कहीं भी लाया लेजाया जाने लागा| इनकी कार्य क्षमता पहले से भी बढ़ गयी|
- इन्टरनेट ने कम्प्युटर की दुनिया में क्रांति ला दिया| आज सारा विश्व मानों जैसे एक छोटे से कम्प्युटर में समा सा गया है| विश्वजाल (World Wide Web) के जरिये संदेशों एवं जानकारी का आदान-प्रदान बेहद ही आसान हो गया, चंद सेकंड्स में ही दुनिया के किसी भी छोर से संपर्क साधना सम्भव हो सका|
- कम्प्युटर की उत्पादन लागत में भारी कमी आने के फलस्वरूप कम्प्युटर की पहुँच घर-घर तक होने लगी है| इनका उपोग हर क्षेत्र में होंने लगा|
- इस पीढ़ी का विकासक्रम अभी भी चल रहा है और कम्प्युटर जगत नए-नए आयाम को छूने की ओर अब भी अग्रसर है|
- इस पीढ़ी के कम्प्युटर ने अपना आकर बेहद ही कम कर लिया है, पाल्म् टॉप, मोबाइल तथा हैण्डहेल्ड जैसे उपकरण तो अब हमारे हथेली पर समाने लगे है|
कम्प्युटर - वर्गीकरण
वर्तमान समय में कम्प्युटर हर सम्भव कार्य करने में सक्षम हैं, जहाँ ये रोजमर्रा के कार्य जैसे दस्तावेज तैयार करना, किसी कार्य का आंकलन करना आदि कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ जटील से जटील वैज्ञानिक कार्य बड़ी ही सहजता से कर जाते है|
हालाँकि अब तक कम्प्युटर का वर्गीकरण उसकी संरचना, कार्यप्रणाली, कार्यक्षमता एवं उसके आकार-प्रकार के आधार पर किया जाता रहा है| वहीं कल तक जो क्षमता मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कम्प्युटर या वर्क स्टेशन की होती थी आज का निजी कम्प्यूटर (Personal Computer) उतना ही या और भी अधिक सामर्थ्यवान बन गया है, और बाकि और भी ज्यादा शक्तिशाली हा चुके हैं| कम्प्युटर की संरचना, कार्यक्षमता और कार्यप्रणाली में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसके मद्देनजर कंप्युटर को एक वर्ग विशेष की परिधि में सिमित करना अनुचित ही होगा| मुख्य रूप से जाने जाने वाले कम्प्युटर में पर्सनल कम्प्युटर, नोटबुक कप्यूटर, पॉकेट कम्प्युटर, पामटॉप कम्प्युटर, वर्कस्टेशन कम्प्युटर, मैनफ्रेम कम्प्युटर तथा सुपर कंप्युटर ईत्यादी आते हैं|
फिर भी कम्प्यूटर को बेहतर समझ सके इसलिए कम्प्युटर के प्रमुख तीन वर्ग इस प्रकार है :
I] संरचना पर आधारित :
१) अनुरूप कंप्यूटर (Analog computer) -
एक कंप्यूटर या गणनात्मक यंत्र जिसमें चर समस्या को सतत रूप से भौतिक मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है|
अनुरूप कंप्यूटर अध्ययन किये जा रहे प्रणाली का एक मॉडल तैयार करता है। अनुरूप कंप्यूटर में सभी प्रचालन समानांतर तरीके से होते है| दूसरी तरफ, अनुरूप कम्प्युटर में डाटा विद्युत दाब के रूप में दर्शाए जाते हैं, जो की सघन परन्तु संचयन के लिए पुष्ट नहीं होता, इसमें शोर से दूषित होने की संभावाना बनी रहती है| डिजिटल कंप्यूटर में एक ट्रांजिस्टर के उपयोग की तरह, अनुरूप कंप्यूटर में संधारित्र (Capacitor) एक सतत चर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं| इनका उपयोग मुक्य रूप से तकनिकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है|
हालाँकि अब तक कम्प्युटर का वर्गीकरण उसकी संरचना, कार्यप्रणाली, कार्यक्षमता एवं उसके आकार-प्रकार के आधार पर किया जाता रहा है| वहीं कल तक जो क्षमता मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कम्प्युटर या वर्क स्टेशन की होती थी आज का निजी कम्प्यूटर (Personal Computer) उतना ही या और भी अधिक सामर्थ्यवान बन गया है, और बाकि और भी ज्यादा शक्तिशाली हा चुके हैं| कम्प्युटर की संरचना, कार्यक्षमता और कार्यप्रणाली में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसके मद्देनजर कंप्युटर को एक वर्ग विशेष की परिधि में सिमित करना अनुचित ही होगा| मुख्य रूप से जाने जाने वाले कम्प्युटर में पर्सनल कम्प्युटर, नोटबुक कप्यूटर, पॉकेट कम्प्युटर, पामटॉप कम्प्युटर, वर्कस्टेशन कम्प्युटर, मैनफ्रेम कम्प्युटर तथा सुपर कंप्युटर ईत्यादी आते हैं|
फिर भी कम्प्यूटर को बेहतर समझ सके इसलिए कम्प्युटर के प्रमुख तीन वर्ग इस प्रकार है :
I] संरचना पर आधारित :
१) अनुरूप कंप्यूटर (Analog computer) -
एक कंप्यूटर या गणनात्मक यंत्र जिसमें चर समस्या को सतत रूप से भौतिक मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है|
अनुरूप कंप्यूटर अध्ययन किये जा रहे प्रणाली का एक मॉडल तैयार करता है। अनुरूप कंप्यूटर में सभी प्रचालन समानांतर तरीके से होते है| दूसरी तरफ, अनुरूप कम्प्युटर में डाटा विद्युत दाब के रूप में दर्शाए जाते हैं, जो की सघन परन्तु संचयन के लिए पुष्ट नहीं होता, इसमें शोर से दूषित होने की संभावाना बनी रहती है| डिजिटल कंप्यूटर में एक ट्रांजिस्टर के उपयोग की तरह, अनुरूप कंप्यूटर में संधारित्र (Capacitor) एक सतत चर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं| इनका उपयोग मुक्य रूप से तकनिकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है|
२) अंकीय कंप्यूटर (Digital computer) -
अंकीय कंप्यूटर एक ऐसा विद्युतीय गणनात्मक उपकरण है, जो कि संख्यात्मक अथवा प्रतीकात्मक जानकारी को निर्दिष्ट गणनात्मक प्रक्रियाओं के अनुरूप बदलता है| अंकीय कंप्यूटर, सभी प्रकार के सूचनाओं को आतंरिक रूप से संख्यात्मक रूप में दर्शाने के लिए द्विआधारी अंकों (बिट्स) 0 और १ का इस्तेमाल करता है| सभी आधुनिक कम्प्युटर जैसे निजी कम्प्युटर, नोटबुक कप्यूटर, पॉकेट कम्प्युटर, पामटॉप कम्प्युटर, वर्कस्टेशन कम्प्युटर, मैनफ्रेम कम्प्युटर तथा सुपर कंप्युटर अंकीय कम्प्युटर के ही प्रकार हैं|
३) संकर कम्प्युटर (Hybrid computer) -
संकर कम्प्युटर एक प्रकार का मध्यवर्ती उपकरण है, जो एक अनुरूप (Analog) output को मानक अंकों (Digital) में परिवर्तित करता है| इनमें अनुरूप तथा अंकीय इन दोनों प्रकार के संगणकों की विशेषताएँ होती है|
संकर कंप्यूटर में, पहले एक अनुरूप कंप्यूटर का इस्तेमाल अग्रांत रूप से बेहतरीन लेकिन अपेक्षाकृत अपरिपक्व आंकडा प्राप्त करने के लिए किया जाता है| तत्पश्चात उससे मिले परिणाम को डिजिटल कम्प्यूटर में वांछित विशुद्ध परिणाम पाने के लिए भरा जाता है| इनका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है, इनकी सहायता से मरीजों के तापमान, रक्तचाप जैसी हलचलों पर निगरानी रखी जाती है|
II] कार्यक्षमता तथा आकार पर आधारित :
१) महा संगणक (Super computer): "महा संगणक" सर्वाधिक शक्तिशाली एवं तीव्र होते है| "महा संगणक" यह शब्द ही अपने आप में परिवर्तनशील है, क्योंकि आज के महा संगणक कल के साधारण कंप्यूटर बन जाता है, तथा मौजूदा महा संगणक और भी अधिक शक्तिशाली बन जाते है|
महा संगणक का इस्तेमाल उच्चस्तरीय सघन गणनात्मक कार्यों के लिए - जिनमें यांत्रिक भौतिकी समस्याएँ, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु शोध, आण्विक मॉडलिंग (रासायनिक यौगिकों, जैविक अणुओं, polymers के गुणों और क्रिस्टल के संरचना एवं गुणों की गणना), भौतिक सिमुलेशन अनुकार (जैसे हवाई सुरंगों में हवाई जहाज के अनुकरण, परमाणु हथियारों के विस्फोट के अनुकार, और अनुसंधान परमाणु संलयन में), और कई दूसरों की. विश्वविद्यालय, सैन्य एजेंसियों और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किया जाता हैं|
२) बृहत संगणक (Mainframe computer): आधुनिक "बृहत्" कंप्यूटर" अपनी एकल संगणनात्मक कार्यगति एवं क्षमताओं के लिए नहीं अपितु, आंतरिक इंजीनियरिंग और उच्च विश्वसनीयता एवं व्यापक सुरक्षा, व्यापक निवेश, उत्पादन सुविधाएं, पुराने सॉफ्टवेयर के साथ संगतता, और उच्चदर्जीय उपयोग का भारी समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं| कार्यक्षमता में ये महा संगणक की अपेक्षा कम, फिर भी शक्तिशाली होते हैं| बृहत् संगणक अपनी सर्वोच्च उपलब्धता के लिए जाने जाते हैं, जो की दीर्घकालीन समय तक कार्य करनें के लिए उपलब्ध रहते हैं| बृहत् संगणक, मुख्य रूप से बड़े संगठनों द्वारा, आम तौर पर अत्यधिक आंकडों जैसे की जनगणना, बड़े-बड़े उद्योग और उपभोक्ता आँकड़े, ERP जैसे प्रसंस्करण, और वित्तीय लेनदेन प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किये जाते है|
३) लघु संगणक (Mini Computer): "लघु संगणक" एक औसत दर्जे का बहुउपयोक्ता संगणक होता है, जो की बृहद संगणक से कम शक्ति वाला और सूक्ष्म संगणक से अधिक शक्तिशाली होता है| जहाँ १९७० और ८० के दशक में बृहद संगणक विकसित हुए; वहीँ लघु संगणक, कम शक्ति वाले सूक्ष्म संगणक और उच्च क्षमता वाले बृहद संगणक के बीच की कमी को भर दिया| इनका आकर बृहत् संगणक से काफी छोटा, तकरीबन एक फ्रिज के आकार जितना होता है|
४) कार्य-केन्द्र (Workstation ): कार्य-केंद्र (वर्कस्टेशन) संगणक एक उच्चस्तरीय सूक्ष्म संगणक है, जो तकनीकी या वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए परिकल्पित किया गया है| ये मुख्यतः एक बार में एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले होते हैं, परन्तु आमतौर पर एक स्थानीय संजालक्रम (Local Network) से जुड़े हुए रहते हैं , तथा बहु उपयोगकर्ता परिचालानतंत्र (Multiuser Operating System)पर कार्य करते है| किसी भी प्रकार के कार्य करनें के लिए कई लोग इनका उपयोग एक ही समय पर, पर एक ही साथ कर सकते है| इनका उपयोग बैंकों में, रेलवे आरक्षण में, विमान उड्डयन स्थल पर, सरकारी कार्यालयों जैसे स्थानों पर किया जाता है|
५) सूक्ष्म संगणक (Micro computer): एक छोटा अंकीय संगणक, जिसका "केंद्रीय संसाधित इकाई" (CPU-central processing unit), जो सूक्ष्म-संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) के डिज़ाइन पर आधारित होता है| यह एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए होता है| जिस आधार पर इसे व्यक्तिगत संगणक के नाम से भी जाना जाता है| कभी बड़े संगणकों से कम शक्तिशाली सूक्ष्म-संसाधित्र (microcomputers), अब कुछ साल पहले के लघु-संगणक (minicomputers) तथा महा-संगणक (supercomputers) से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं| सूक्ष्म-संगणक का प्रभावशाली प्रौद्योगिक तकनिकी, व्यक्तिगत संगणक तथा कार्य-स्थल संगणक के विकास के पीछे प्रमुख रूप से रहा है| इनमें कुंजीपटल, दृश्यपटल तथा माउस, ईत्यादी का उपयोग निर्गम-निवेश (Input/Output) के लिए किया जाता है|
III] अंत:संबंधन पर आधारित :
१) वितरित संगणक तंत्र (Distributed computer system): वितरित संगणक तंत्र में कई स्वायत्त संगणक शामिल होते हैं जो की एक संगणक संजालक्रम के माध्यम से जुड़े रह कर एक दुसरे से संपर्क स्थापित करते हैं| इस प्रणाली में प्रत्येक कंप्यूटर एक आम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं| वितरित अभिकलन संरचना, समवर्ती प्रक्रियाओं के कार्यों में संचार और समन्वय बैठाने की विधि है| एक वितरित प्रणाली में चलने वाले संगणक प्रोग्राम को वितरित प्रोग्राम कहा जाता है, और वितरित प्रोग्रामिंग ऐसे प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया है।
वितरित अभिकलन, गणनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए वितरित प्रणाली का उपयोग करता है. वितरित अभिकलन में, एक समस्या का विभाजन कई कार्यों में कर, हर एक कार्य को एक निजी कंप्यूटर द्वारा हल किया जाता है| तत्पश्चात सभी हलों को एकत्रित कर निष्कर्ष निकला जाता है|
२) समानांतर संगणक तंत्र (Parallel computer system): समानांतर कंप्यूटर में आमतौर पर, एक ही बहु-प्रक्रमक संगणक के हार्डवेयर उसके बहु-केन्द्रित एवं बहु-प्रचालन तंत्र के साथ समन्वय बनाकर समानता स्थापित करता है| इस कार्य के लिए विशेष प्रकार के सामानांतर प्रचालन तंत्र (Parallel Operating Programs) का उपयोग किया जाता है|
समानांतर संगणक तंत्र , एक समस्या को हल करने के लिए कई संसाधन इकाई का एक ही साथ उपयोग करता है। सवालों को कई स्वतंत्र भागों में बाँट दिया जाता है, जिससे प्रत्येक प्रसंस्करण अपने हिस्से के अभिकलन को दूसरों के साथ ही साथ पूरा कर सकें| समानांतर संगणक तंत्र , में कई गणना एक साथ हल किए जाते हैं, कई बड़े-बड़े सवालों को छोटे हिस्सों में बाँट कर उन्हें एक ही साथ अलग-अलग हल किया जाता है|
कम्प्युटर - संरचना
कम्प्युटर कई तरह के कलपुर्जों, अर्थात Hardware एवं प्रक्रिया सामग्री अर्थात
Software के परस्पर समन्वयन से बनता है| सारे कल-पुर्जे (Hardwares) आपस
में, एक-दुसरे से जुड़ कर कम्प्युटर का ढांचा तैयार करते हैं, और प्रकिया
सामग्री (Softwares) हर पुर्जों से उनके लिए निर्दिष्ट कार्य करवाती है|
कम्प्युटर बनाने के लिए प्रयोग में आने वाले प्रमुख कल-पुर्जे (Hardwares) इस प्रकार है :-
कम्प्युटर बनाने के लिए प्रयोग में आने वाले प्रमुख कल-पुर्जे (Hardwares) इस प्रकार है :-
१) केन्द्रीय प्रचालन तंत्र (CPU -Central Processing Unit, Processor):
इसे माईक्रोप्रोसेसर भी कहते हैं, यह कम्प्युटर का प्रमुख अंग होता है| माईक्रोप्रोसेसर में ही उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट सभी निर्देशों पर कार्य किया जाता है, प्रोसेसर के तीन मुख्य खंड होते हैं, CU-कंट्रोल युनिट, ALU- अरिथमटिक एंड लोगिकल युनिट, तथा MU- मेमोरी युनिट| कंट्रोल युनिट सारी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है तथा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य को ALU या MU को वितरित करता है, तत्पश्चात उनके द्वारा दिए परिणाम को आगे भेजता है| इसे कम्प्युटर का मष्तिष्क भी कहा जाता है| इनकी कार्य-क्षमता किलोहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ तथा गिगाहर्ट्ज़ आदी में नापी जाती है|
प्रोसेसर की कार्य-प्रणाली को बिट के आधार पर आँका जाता है, जैसे की ८-बिट, १६-बिट, ३२ -बिट एवं ६४-बिट। हर एक बिट में दो मान होते हैं (०० या ०१ या १० या ११) इस प्रकार ३२-बिट में कुल २३२ तक मान होते हैं। ३२-बिट प्रोसेसर एक समय में कुल २३२ तक के आंकडों पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। एक प्रोसेसर में जितने अधिक बिट होंगे उनके कार्य करने की क्षमता एवं सटीकता उतनी ही प्रभावशाली होगी। ३२ -बिट प्रोसेसर ३२ -बिट एवं उससे कम क्षमता तक के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर ही कार्य कर सकता है ३२ -बिट प्रोसेसर ६४-बिट क्षमता के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर कार्य नहीं कर सकता। जबकि ६४-बिट प्रोसेसर ३२ -बिट एवं उससे कम क्षमता तक के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर कार्य कर सकता है।


२) यादृच्छिक अभिगम स्मृति ( RAM-Random Access Memory):
RAM कम्प्युटर की अस्थाई स्मृति होती है, ये कम्प्युटर के प्राथमिक संग्रहण उपकरण होते हैं| इनका CPU के साथ सीधा संपर्क होता है, उपयोगकर्ता द्वारा भरी गई जानकारी तथा निर्देश ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्वप्रथम RAM में आती है, फिर किसी भी जानकारी को CPU जरुरतानुसार RAM से लेता है, तथा क्रियान्वयन के पश्चात् उसे पुन: RAM के पास भेज देता है, जहाँ से उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रहण कर लेता है| RAM की स्मृति क्षणभंगुर होती है, जब तक कम्प्युटर में विद्युत प्रवाहित होता है, RAM की स्मृति तभी तक बनी रहती है, जैसे ही विद्युत प्रवाह खंडित होता है, RAM की स्मृति नष्ट हो जाती है परिणामस्वरूप उसमे स्थित सारी जानकारी लुप्त हो जाती है| इनकी क्षमता किलो बाईट, मेगाबाईट तथा गिगाबाईट आदी में नापी जाती है|
३) मुख्य तंत्र पटल (Main\System\Mother Board):
यह कई नामों से जाना जाता है जिनमे, मदरबोर्ड, सिस्टमबोर्ड तथा मैनबोर्ड ये ज्यादा चलन में है, कई बार इन्हें प्लानर भी कहा जाता है| ये एक प्रकार के सर्किटबोर्ड होते हैं जिनसे अन्य सभी पुर्जे एक विशेष प्रणाली के तहत परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आपस में जुड़े हुए रहते है, जिससे सभी पुर्जों के बिच लगातार परस्पर समन्वयन एवं संवाद स्थापित रहता है| माइक्रोप्रोसेसर, RAM, चिपसेट, ग्राफिक कंट्रोलर, अन्य इनपुट-आउटपुट कंट्रोलर मदर बोर्ड पर ही स्थापित्य किये हुए होते हैं| इनकी कार्यक्षमता नापने की इकाई FSB (फ्रंट साइड बस) होती है|
४) अनम्यिका (HDD -Hard Disk):
ये कम्प्युटर के स्थाई स्मृति होते हैं| इनपर स्थापित किये गए जानकारी सदा के लिए बने रहते है| ये कम्प्युटर के द्वितीयक संग्रहण उपकरण होते हैं| इनकी क्षमता RAM से कहीं ज्यादा होती है, और ये ढेरों जानकारी संग्रह कर रखने में सक्षम होते हैं| ये RAM की तरह क्षणभंगुर नहीं होते, तथा विद्युत संचार बंद होने के बाद भी इनपर रक्षित की गयी जानकारी बनी रहती है| इन पर रक्षित की गयी जानकारी अमिट होती है, वे तभी मिटती हैं जब उपयोगकर्ता खुद उन्हें मिटाना चाहें| ये मदर बोर्ड के IDE (ATA) अथवा SATA कंट्रोलर से जुड़े होते हैं| इनकी क्षमता मेगाबाईट, गिगाबाईट, टेराबाईट, पीकाबाईट आदी में आंकी जाती है| यह कम्प्युटर में स्थायी रूप से बने रहते हैं इसीलिए दस्तावेज आदान-प्रदान के लिए सामान्यतया इन्हें एक कम्यूटर से निकाल कर दुसरे कम्प्युटर में नहीं लगाया जाता|
ये कम्प्युटर के स्थाई स्मृति होते हैं| इनपर स्थापित किये गए जानकारी सदा के लिए बने रहते है| ये कम्प्युटर के द्वितीयक संग्रहण उपकरण होते हैं| इनकी क्षमता RAM से कहीं ज्यादा होती है, और ये ढेरों जानकारी संग्रह कर रखने में सक्षम होते हैं| ये RAM की तरह क्षणभंगुर नहीं होते, तथा विद्युत संचार बंद होने के बाद भी इनपर रक्षित की गयी जानकारी बनी रहती है| इन पर रक्षित की गयी जानकारी अमिट होती है, वे तभी मिटती हैं जब उपयोगकर्ता खुद उन्हें मिटाना चाहें| ये मदर बोर्ड के IDE (ATA) अथवा SATA कंट्रोलर से जुड़े होते हैं| इनकी क्षमता मेगाबाईट, गिगाबाईट, टेराबाईट, पीकाबाईट आदी में आंकी जाती है| यह कम्प्युटर में स्थायी रूप से बने रहते हैं इसीलिए दस्तावेज आदान-प्रदान के लिए सामान्यतया इन्हें एक कम्यूटर से निकाल कर दुसरे कम्प्युटर में नहीं लगाया जाता|
५) सघन चक्रिका चालन (CD \ DVD Rom - Compact \ Video Disc Drive):
हार्ड डिस्क के विपरीत कॉम्पेक्ट डिस्क आसानी से निकाले जाने लायक होते है एवं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाये ले जाए जा सकते हैं जिससे दस्तावेजों का आदान-प्रदान आसानी से किया जाता है|
६) नम्यिका (FDD - Floppy Disk Drive):
७) दृश्यपटल यंत्र / प्रदर्श (Monitor):
८) कुंजीपटल यन्त्र (Keyboard):
९) माउस (Mouse):
१०) पॉवर सप्लाई :
११) तंत्र पेटिका (System Cabinet ):
प्रक्रिया सामग्री (Softwares) के प्रकार :-
१) तंत्र प्रक्रिया सामग्री (System Softwares) : सिस्टम सॉफ्टवेयर कम्प्युटर के सभी अंगों का CPU के साथ सामंजस्य बैठाकर हर पुर्जों से उनके लिए निर्दिष्ट कार्य करवाता है| ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है| ये उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदल कर CPU को देता है, और जब CPU उन निर्देशों को कार्यान्वित कर के परिणाम देता है तो उस परिणाम को मशीनी भाषा से पुन: हमारे समझने लायक भाषा में बदल कर दर्शाता है| माइक्रोसॉफ्ट विन्डोज़, लिनक्स, एप्पल मकींटोश, यूनिक्स आदि प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं| ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेर के बिच सामंजस्य स्थापित करता है|
२) अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री (Aplications Softwares): ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग दैनदिन होने वाले कार्यों को करनें के लिए किया जाता है| हर तरह के कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं| दस्तावेज तैयार करने तथा संपादित करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेर होता है| हिसाब-खिताब रखने तथा बही-खता बनाने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है| छवि तथा चलचित्र का संपादन करने के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं|
Computer parts Knowledge in Hindi (कंप्यूटर पार्ट्स)
Computer Parts
 |
| computer parts |
कंप्यूटर हार्डवेयर Computer hardware को समझने के लिए हमे उनके पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी हैं|
कंप्यूटर में मुख्य रूप से निम्न पार्ट्स होते हैं।
Micro Processor प्रोसेसर : Computer parts Knowledge in Hindi (कंप्यूटर पार्ट्स)
माइक्रोप्रोसेसर जिसको सीपीयू भी कहा जाता है एक चिप की तरह होती है जिसे मदरबोर्ड पर सीपीयू सॉकेट में लगाया जाता है। कंप्यूटर की स्पीड सीपीयू पर ही निर्भर होती है। इसलिए हमेशा कंप्यूटर लेते समय सीपीयू पर ध्यान देना चाहिए। सीपीयू Intel AMD कंपनी के मिलते है।Mother Board मदर बोर्ड : Computer parts Knowledge in Hindi (कंप्यूटर पार्ट्स)
सीपीयू cpu के अनुसार मदरबोर्ड का चुनाव किया जाता है। आपको वही मदरबोर्ड लेना चाहिए जो आपके सीपीयू को सपोर्ट करता हो। यह एक समतल बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स सॉकेक्ट कनेक्टर लगे होते है। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मदरबोर्ड पर जोड़े जाते है। यह भी बहुत कम्पनियो के द्वारा बनाये जाते है जैसे : Intel Motherboard, Asus Motherboard, Gigabyte Motherboard, MSI Motherboard, Zebronics Motherboard और chines Motherboard .Memory मेमोरी
Memory जिसे रैम ( Random Access Memory) कहा जाता है। पतली पीसीबी(PCB) पर कुछ कंपोनेंट्स लगे होते है। सीपीयू सारे काम रैम के द्वारा ही संम्पन करता है बिना इसके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आएगी। कंप्यूटर की काम करने की स्पीड सीपीयू के बाद रैम पर निर्भर करता है। यह कई कैपेसिटी के आती है। Kingston Ram 1GB, 2GB, Simtronics Ram, hynics, IBM ectHard Disk Drive हार्ड डिस्क
हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस (storage Device ) होती है , जिसमे कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर फाइल Audio, Video, Image Files आदि को Store किया जाता है, कंप्यूटर की विंडो या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर HDD में ही Install की जाती है , इसकी Capacity जितनी ज्यादा होगी। उतना ज्यादा डेटा रख सकते है . पर्सनल कंप्यूटर में यह दो Types में आती है IDE और SATA . Sata HDD की Speed ज्यादा होती है। samsung hard disk, segate hdd, WD hard disk drive---160 GB, 250 GB, 320 GB, 500GB, 1TB, 10 TBCD/DVD Drive सी.डी रोम
यह एक ऑप्टिकल ड्राइव प्लेयर(optical Drive Player) होती है। जिसमे CD डीवीडी को चलाया जाता है। CD के द्वारा कंप्यूटर में विंडो डालने गेम्स सॉफ्टवेयर इनस्टॉल करने तथा CD से Films देखने आदि काम किये जाते है , यदि Cd राइटर है तो आप Blank CD को Write भी कर सकते है , LG DVD WRITER, HP, SONY, ASUS DVD WRITERModem मॉडेम : Computer parts Knowledge in Hindi (कंप्यूटर पार्ट्स)
modem के द्वारा कंप्यूटर को Internet से Connect के लिए होता है। यह दो तरह के होते है , Internal और External। लेकिन अब USB Data Card का उपयोग बहुत किया जाता हैSound Card साउंड कार्ड
साउंड कार्ड के द्वारा कंप्यूटर को स्पीकर से जोड़ा जाता है। साउंड की क्वालिटी और परफॉमेंस साउंड कार्ड पर निर्भर करता है। ज्यादातर मदरबोर्ड में साउंड कार्ड पहले से ही लगे होते होते हे लेकिन अलग से भी साउंड कार्ड को मदरबोर्ड में Install किया जा सकता है।Monitor मॉनिटर
मॉनिटर का काम कंप्यूटर के सारे काम को Screen पर दिखाना होता है। यह दो तरह के होते है। CRT और LCD . यह बहुत से साइज में आते है LG Monitor. Samsung Lcd monitor, BenQ, HP, Sony, IntexKeyboard/Mouse की-बोर्ड माउस
Keyboard पर बहुत सारे बटन होते है , जिनको दबाकर कंप्यूटर में instraction दिया जाता हैहै , जिससे कंप्यूटर काम करता है। माउस ऑप्टिकल डिवाइस होता है। इस पर दो buttons लगे होते है। मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर के द्वारा कंप्यूटर में काम किया जाता है।Speaker
स्पीकर के द्वारा कंप्यूटर साउंड को सुनने इसका उपयोग करते हैPrinters
प्रिंटर कंप्यूटर के डेटा को प्रिंट Print करता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने लैपटॉप(Laptop) या पीसी (PC) का पावर बटन दबाते हैं, तब से लेकर विंडो(Window Xp, Window 7, Window 8, Linux) का लोगों आने तक क्या होता है। आप देखते है की स्क्रीन पर हज़ारो लाइने तेज़ी से चलती दिखाई देती है।
असल में कंप्यूटर अंपने आप को स्कैन (scan) करता है। जिसमे न जाने कितने
कॉम्पोनेंट्स काम करते है। यह काम सीपीयू के और बायोस के द्वारा किया जाता
है। इस प्रक्रिया को पोस्ट(Post) कहा जाता है।
बूटिंग क्या होता है। What Is Booting ?
जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया को पूरी कर लेता है तब विंडो को लोड करने
का काम करता है। जिसके लिए यह बायोस(Bios) के प्रोग्राम के अनुसार हर बूट
डिवाइस में बूटिंग फाइल देखता है।
"असल में बूटिंग एक अनुक्रम (Sequence) होता है। जो बायोस प्रोग्रामर
के द्वारा पहले से ही बायोस में स्टोर रहता है। इस प्रक्रिया में एक-एक
करके बूटिंग डिवाइस को कंप्यूटर ढूंढ़ता है "
जिस डिवाइस(Device) में बूटिंग फाइल(Booting File) मिल जाती है। तो कंप्यूटर विंडो लोडिंग शुरू कर देता है।
निर्माता के द्वारा पहला बूट डिवाइस Floppy Disk Drive को बनाया जाता है।
लेकिन यूजर(User) अपने अनुसार बायोस में बूटिंग का डिवाइस को चुन सकता है।
Default Boot Option In CMOS/BIOS SETUP
 |
| Bios Set-up Boot option Screenshot |
First Boot Device - Floppy
Second Boot Device - HDD 0
Third Boot Device - CDROM
Boot Other Device - Enabled
कंप्यूटर को हार्ड डिस्क से बूट कराया जाता है क्यूंकि हार्ड डिस्क में ही विंडो को इनस्टॉल करते है। यदि हार्ड डिस्क में विंडो इनस्टॉल है तो फर्स्ट बूट डिवाइस(First Boot Device) कोई भी हो कंप्यूटर हार्ड डिस्क से बूट हो जायेगा।
बूटिंग ऑप्शन को बदले की जरुरत क्यों पड़ती है।
यदि किसी कंप्यूटर में दो या अधिक हार्ड डिस्क लगी है। और दोनों में विंडो इनस्टॉल है। मान लीजिये HDD1 और HDD2 लेकिन आपको HDD2 से कंप्यूटर को बूट करना है तो आपको फर्स्ट बूट डिवाइस में HDD2 को फर्स्ट बूट करना पड़ेगा नहीं तो प्योरिटी में जो पहले होगा उससे ही कंप्यूटर बूट कर जायेगा।विंडो इनस्टॉल करते समय :
जब किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में नयी विंडो डाली जाती है तो आप जिस डिवाइस से विंडो डालते है उसको फर्स्ट बूट बनाना पड़ता है।यदि आप cd से विंडो डालते है तो cd को बायोस में जाकर बूट ऑप्शन में cdrom को फर्स्ट बूटिंग डिवाइस बनाना पड़ेगा।
इसी तरह से Pen Drive , usb cdrom, usb hdd , Lan जिस डिवाइस से विंडो इनस्टॉल करनी है उसे फर्स्ट बूट पर सेट करना होगा तभी कंप्यूटर उस डिवाइस से बूट करेगा नहीं तो , कंप्यूटर हार्ड डिस्क से बूट कर जायेगा। या फिर Insert Boot Media Disk का Error Message Screen पर दिखाई देगा। यह मैसेज तब भी आएगा यदि आप जिससे विंडो डालना चाहते है वह बूटेबल नहीं होगा या सही से Bootable बना नहीं होगा।
बायोस सेटअप में जाने के लिए कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही Del, F2, Ctrl+Alt दबाते है। बायोस निर्माता के अनुसार अलग अलग होते है।




































































0 comments:
Post a Comment